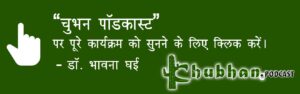 -डॉ. श्रीलता सुरेश
-डॉ. श्रीलता सुरेश
भारत की समृद्ध संस्कृति प्राचीन काल से हैl उच्चतम मानवीय मूल्यों को पूरे विश्व में स्थापित करने के लिए विख्यात रहा हैl भारत देश साधु-संतों का देश हैं।संत- परंपरा हमारे देश का आध्यात्मिक वैभव है।धर्म के कारण यह संतों के कार्य का मुख्य उद्देश्य है।संतों ने साहित्य और धर्म समाज सुधार में भी बड़ा योगदान दिया है।समाज को निरंतर जगाने का कार्य विभिन्न राज्यों के अनेक संतों ने किया हैl समाज-जागरण के इस कार्य के लिए संतों के उपकारों को जितना मानें उतना कम है। इन में भी कर्नाटक में भक्ति का उद्भव हुआ है और धर्मों के बोधक, धर्मोपदेशक और महान आत्मा इस पावन भूमि पर अवतरित हुए हैं।इन महात्माओं ने आदर्श-जीवन मूल्यों, आचार-विचार कर्मण्यता, सौहार्दता और अन्य विषयों को लेकर समय-समय पर सचेत करने का प्रयास किया है। इनकी शिक्षाओं और उपदेशों से जो मूल बात उभरती है, वह यह है कि इन सभी संतों के सन्देश के केंद्र में मानव कल्याण का भाव है।
9वी से लेकर 12वी शताब्दी के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तक कर्नाटक की सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक स्थिति संकटों से भरी रहीl होयसाला राजाओं की अवनति के साथ छोटे-बड़े राजा अपने-आप को स्वतंत्र समझकर एक-दूसरे से विरोध करते रहे। इससे उत्तर भारत के मुसलमान राजाओं को फायदा हुआ।अलाउद्दीन जैसे अनेक मुसलमान शासकों ने आकर आक्रमण से, लूटपाट, अशांति और अव्यवस्था पैदा की।
दक्षिण भारत के कर्नाटक में भक्ति की दो धाराएं प्रमुख रूप से प्रचलित हैं।वीर शैव संप्रदाय की शिव भक्ति धारा एवं वैष्णव संप्रदाय की विष्णु धारा। दोनों सम्प्रदायों के संतों ने, समाज में सुधार और भक्ति-भाव के प्रसार की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए हैं।
इन संतों की विशिष्टता के बारे में कहा जा सकता है कि गूढ़ दार्शनिक तत्वों को भी सर्व जनों के लिए ग्राह्य बनाने के लिए इन महान पुरुषों ने जनता को सरल भाषा में साहित्य की अनेक विधाओं में कृतियाँ रचकर लोगों तक पहुंचाने का परोपकार किया है।

अल्लाम्मा प्रभु, बारहवीं शताब्दी के कन्नड़ के एक बहुत प्रतिभाशाली लिंगायत संत थे, जो स्वयं आत्मा के महत्व को समझते थे और लोगों की आत्मा में आध्यात्मिक ऊर्जा भरते थे। कहा जाता है कि वे कर्नाटक राज्य में एक मंदिर में कार्यरत थेl उनकी पत्नी के निधन के वियोग में वे एक गुफा मंदिर में गए जहाँ एक संत के आशीर्वाद के बाद स्वयं संत बन गएl भागवत ज्ञान का आशीर्वाद पाकर , अल्लामा को आध्यात्मिकता के साधक के रूप में बदल दिया। अल्लामा प्रभु की अध्यात्मिक शक्तियों से मंदिर की पूजा और धार्मिक प्रथाओं पर केन्द्रित किया। इन्होंने लगभग 1300 से भी अधिक भक्ति गीतों का सृजन किया है।उनकी कविताओं में शिव को संदर्भित करने के लिए “गुफाओं के भगवान” या “गुएश्वरा” वाक्यांश का उपयोग किया गया है।वे एक अध्यात्मिक सुधारक और महान संत थे, जो लोगों के कल्याण के लिए, गरीब लोगों के उत्थान के लिए जीवन बिताए। लोगों के बीच पूजा का आह्वान किया और उनसे अपने शरीर में भगवान शिव का लिंग के रूप में मूर्ति धारण करने के लिए कहा। उनका मानना था कि पूरी प्रकृति एकता और सामंजस्य के दर्शन से आनंद से अभिभूत है। ऊपर से अलग- अलग दिखने वाली चीजें भीतर से एक ही हैंl उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए अपना अधिकतर जीवन गरीब लोगों के उत्थान में बिताया।
संत बसवेश्वर का जन्म 1131 ईसवीं में कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित बागेवाड़ी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था।उस समय ऊँच-नीच, जातिप्रथा का भेदभाव बहुत था। एक बार उन्होंने अपने उपनयन संस्कार के बाद अपनी जनेऊ को उतार दिया था और इस तरह जातिप्रथा पर आधारित समाज के बदले में कर्म पर आधारित समाज व्यवस्थाओं पर अधिक बल दिया।
बासव के चाचा प्रधानमंत्री थे और इनको कोषागार प्रमुख के रूप में नियुक्त किया था। उनके काल में समाज ऐसे चौराहे पर खड़ा था, जहाँ चारों ओर धार्मिक पाखण्ड, जात-पात, छुआछूत, अंधश्रद्धा से भरे कर्मकांड और साम्प्रदायिक उन्माद चरम पर था।
मठों, मंदिरों में फैली कुरीतियों तथा अंधविश्वासों की सत्ता को चुनौती दी। सभी वर्ग के लोगों को बराबर अवसर देने की बात कही। उन्होंने कुरीतियों को हटाने के लिए एक नए संप्रदाय की स्थापना की जिसका नाम लिंगायत रखा था। कर्नाटक में हिन्दुओं के मुख्यतः पाँच संप्रदाय माने जाते है- शैव, वैष्णव, शाक्त, वैदिक और स्मार्त के नाम से जाना जाता है।
इन्हीं में एक शिव सम्प्रदाय के कई उप-सम्प्रदाय है, उसमें से एक है वीरशैव सम्प्रदाय।लिंगायत इसी वीरशैव सम्प्रदाय का हिस्सा था। कुछ अभिलेखों के अनुसार यह पहले से ही मौजूद मत था। बसव या बसवान्ना अता बस्वेश्वरा ने इस वीरशैव को पुनर्जीवित कियाl उन्होंने समाज में धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों की रचना की दिशा में कार्य करने के लिए कूडल संगम की स्थापना की।इतना ही नहीं उन्होंने सब के लिए धाम का द्वार खोलकर जाति, लिंग या पंथ आदि के आधार पर भेदभाव का कोई स्थान नहीं दियाl”अनुभव मण्डप” नामक एक सामाजिक और अध्यात्मिक संस्था की स्थापना की जो देश भर के सैकड़ों संतों और अध्यात्मिक साधकों को आकर्षित किया। इनकी लिखी वचनावली आज भी प्रसिद्ध है।
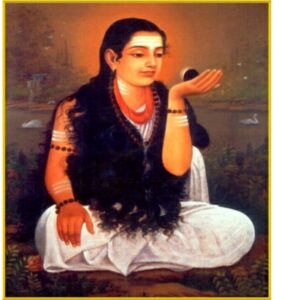
अक्क महादेवी
बारहवीं शताब्दी की प्रख्यात कन्नड़ कवयित्री का जन्म शिवमोगा जिले के शिकारपुर तहसील के एक गाँव में हुआ।बहुत सुन्दर थी, इसीलिए वहां के राजा कौशिक ने उनसे विवाह का प्रस्ताव भेजा।उनके माता-पिता राजा के डर से ठुकरा न सके। विवाह के बाद महादेवी ने कहा कि बचपन में ही “चेन्नामाल्लिकार्जुन (शिव) को अपना पति मान चुकी है।यह समाचार राजा सहन न कर सके और आदेश दिया कि सब कुछ छोड़कर चली जाए। महादेवी ने आभूषण, वस्त्र उतार कर अपने घने और लम्बे बालों से शरीर ढक लिया वहाँ से निकल गई। वह समाज की भर्त्सना की परवाह न करते हुए जंगल-जंगल भटकते हुए बीदर जिले पहुंचीl यह नगर शिव भक्ति में प्रसिद्ध है महादेवि ने “अनुभव मण्डप” की स्थापना कर अध्यात्मिक वचनों से जनता को उजागर किया।उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर आदर पूर्वक उन्हें अक्का यानि दीदी कहने लगे और फिर अक्का महादेवी के नाम से पहचानी जाने लगी।
अक्का महादेवी ने कन्नड़ साहित्य में लगभग 430 वचनों की रचना की है जो भगवान मल्लिकार्जुन के प्रेम और अध्यात्मिक कल्याण पर रचित है। उनकी पवित्र भक्ति इतनी उच्च कोटि की थी कि समाज उनके सामने नतमस्तक हो गया। उनका मानना है कि जड़-चेतन, पशु-पक्षी वन-पर्वत सभी शिवमय है।
(13 वी) शताब्दी मध्वाचार्य :
भक्ति आंदोलन के मुख्य दार्शनिक और आध्यात्मिक चेन में जाग्रति लाने वाले संत मध्वाचार्य जी है। इन्होंने कर्म को मानव जीवन का मूलभूत अंग और सिद्धांत माना है। मनुष्य अपने पुनर्जन्म के कष्टों को कर्म श्रेष्ठता से मुक्ति पा सकता है।उडुपी के निकट तुलुव क्षेत्र में श्रीनारायण भट्ट और श्रीमती वेदवती को विजयदशमी के दिन एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम वासुदेव रखा गया।11 वर्ष के आयु में अद्वैत मत का दीक्षा ली। वेदान्त में पारंगत हो जाने पर इन्हें आनन्दतीर्थ नाम देकर मठाधीश बना दिया गया। बाद में मध्व नाम से प्रख्यात हुए। मध्व को अद्वैतवाद में दीक्षित होने पर भी उनको प्रमुख रूप से कुछ आपत्तियाँ थी। जैसे जीव और ब्रह्म में पार्थक्य होने पर भी अद्वैत माना है और निर्गुण ब्रह्म की संकल्पना मानव को शान्ति प्रदान करने में भी असमर्थ थी।अतः उनका मत यह है कि श्रीविष्णु ही सर्वोच्च तत्व हैं, जगत सत्य हैl ब्रह्म और जीव का भेद वास्तविक है। जीव ईश्वर के अधीन हैं, जीवों में तारतम्य, आत्मा के आंतरिक सुखों का अनुभव ही मुक्ति हैl वास्तविक सुख वह है जिसमें दुःख के क्षय के साथ ही परमानंद का उदय हो जाता है।
श्रीमध्वाचार्य ने सम्पूर्ण भारत का भ्रमण किया और स्थान- स्थान पर शास्त्रार्थ करके विद्वानों में ख्याति अर्जित की। इनके शास्त्रार्थ का मूल भगवद्भक्ति का प्रचार, वेदों की प्रमाणिकता की स्थापना, मायावाद का खंडन तथा शास्त्र-मार्यादा का संरक्षण करना था। गीताशाश्य का निर्माण करने के बाद इन्होंने जब बद्रीनारायण की यात्रा की, वहाँ इनको वेदव्यास के दर्शन हुए।अनेक विद्वानों ने इनसे प्रभावित होकर इनका मत स्वीकार किया। बद्रीनारायण में श्री व्यासजी ने इन पर प्रसन्न होकर इन्हें तीन शालिग्राम शिलाएँ दी थीं।
एक बार की बात है, एक व्यापारी का जहाज द्वारका से मालावार जा रहा था। तुलुब के पास वह ड़ूब गया। उस में गोपीचंदन से ढकी हुई भगवान श्रीकृष्ण की एक मूर्ति थीl मध्वाचार्य को भगवान की आज्ञा प्राप्त हुई और उन्होंने जल मूर्ति निकालकर उडुपी में उसकी स्थापना की, तभी से वह स्थान मध्व मत के अनुसार श्रेष्ठ तीर्थ हो गया।इन्होंने उडुपी में अष्ट मठों की स्थापना की। आज भी लोग उस पावन मंदिर के दर्शन करके जीवन का वास्तविक लाभ प्राप्त करते हैं। मध्वाचार्य ने 37 ग्रंथों की रचना की जिनमें से दो प्रमुख माने जाते है–ब्रह्म सूत्र का भाष्य और उपनिषदों का टीका।
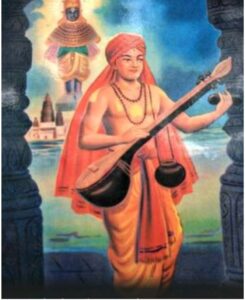
पुरंदरदास
कर्णाटक संगीत के “ भीष्म पितामह” कहलाने वाले संत पुरंदरदास का जन्म शिवमोगा जिले के तीर्थहल्ली में हुआ। इनका नाम श्रीनिवास नायक था। उनके पिता वरदप्पा एक धनी व्यापारी थे।अपनी परंपरा के अनुसार औपचारिक शिक्षा प्राप्त की।वे कन्नड़, संस्कृत और संगीत में भी प्रवीण थे। उनका विवाह सरस्वती नामक युवती से हुआ।वे अपने पिता का धंधा संभालते थे।कहा जाता है कि एक दिन श्रीनिवास के घर एक गरीब ब्राह्मण ने अपने पुत्र की जनेऊ संस्कार के लिए धन देने की कृपा की। श्रीनिवास ने इन्कार कर दिया।निराश होकर जा रहा था तो श्रीनिवास की पत्नी को उस ब्राह्मण पर तरस आया।उसके हाथ में पैसे तो नहीं थे, मगर उसने अपनी नाक की कीमती नथ निकालकर उस ब्राह्मण को दे दीl उस ब्राह्मण ने वह नथ लेकर सेठ श्रीनिवास की दुकान में उसे बेचने गया। श्रीनिवास ने उस नथ को गौर से देखा और संदेह हुआ कि उसकी पत्नी के पास भी यही नथ है।अपना संदेह दूर करने के लिए उस ब्राह्मण को वहीँ दुकान पर बैठाकर जल्दी से घर पहुँचा और अपनी पत्नी को नथ के बारे में पूछने लगा। पत्नी श्रीनिवास के स्वभाव से परिचित होने के कारण जानती थी कि उसे धन अधिक प्यारा था। अहसास था कि श्रीनिवास को पता चलेगा की वह नथ गरीब ब्राह्मण को दे दिया तो उसका परिणाम क्या होगा? डर से उसने विष पीकर प्राण त्यागने का निश्चय किया। तुरंत वह एक कटोरे में विष लेकर ईश्वर की मूर्ति के सामने खड़ी होकर हरि नाम मन में स्मरण करते हुए विष पीने के लिए तैयार होती है, तो उसने देखा और आश्चर्य हुआ कि विष के स्थान पर उस कटोरे में वही नथ पड़ी हुई थी। समझ गई कि यह ईश्वर की लीला है।
यह सब उसके पति, पीछे खड़े हुए देख रहे थे। उनको भी आश्चर्य हुआ। उस नथ को लेकर दुकान पर आकर अपनी तिजोरी खोलकर देखा तो ब्राह्मण का दिया हुआ नथ, जो उसने उसी तिजोरी में रखकर अपने घर गया था, वह नहीं रहा। इस चमत्कार पूर्ण घटना ने श्रीनिवास के चक्षु खोल दिए।
उसके बाद उनके जीवन में बदलाव आ गया।जाना कि अपने जीवन की सार्थकता ईश्वर को जीवन समर्पित करके जीने में ही है।अपनी सारी धन दौलत गरीबों में बाँट कर श्रीनिवास अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मुनि व्यास तीर्थ के मठ पहुँचे। वहाँ पर उनको मंत्रोपदेश दिया, जिसके बाद उनको पुरंदर दास के नाम से जाना गया।वे भगवान की भक्ति में लीन होकर अपने इष्ट देव की याद में नित्य नए गीत या पद रचते और गाकर भक्तों को गदगद किया करते। पुरंदर दास ने अपने गीतों तथा भजनों के द्वारा संगीत को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने चार लाख पचहत्तर हजार(4,75,000) कीर्तनों, यानि भक्ति गीतों की रचना की। उन रचनाओं में से अधिकतर कन्नड़ भाषा में है और कुछ संस्कृत में हैं। उनका दर्शन हिंदू धर्म में भक्ति की अवधारणा का सामंजस्य है l यह भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण आत्म-समर्पण और अगाध प्रेम सिखाता है।
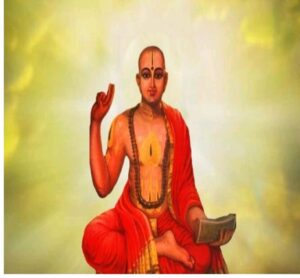
कनकदास
धारवाड़ जिले के ‘बाद’ नामक गाँव में गडरिया जाती में कनकदास का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम बीरेगौड और माता बच्चम्मा थे।इनको अधिक समय तक संतान प्राप्ति न होने के कारण तिरुपति के भगवान बालाजी वेकटेश्वरा की कृपा से एक पुत्र का जन्म हुआ। तिम्मप्पा नामकरण किया गया था। विजयनगर के राजा के पास बीरेगौड सेनापति थे। तिम्माप्पा के बचपन में ही पिता की मृत्यु हो गईl इसलिए उनके सेनापति के कार्यभार को स्वयं निभाना पड़ा।कहा जाता है कि उसे बहुत ही सक्षम होकर निभाया।एक बार तिम्मप्पा भूशोधन करते समय ज़मीन को गाड़ा गया तो धन से भरा हुआ हांडा मिला।उस धन को निर्धन लोगों में और अपने जन्मस्थान बाद में स्थित मंदिर के कार्य में दे दिया। इसलिए इनका नाम कनक हो गया।
इनकी कीर्ति वृद्धि होने लगी। वे विजयनगर साम्राज्य के अधीन सैन्याधिकारी हो गए। लोग उन्हें कनक नायक कहने लगे।कई युद्धों में शौर्य प्रदर्शन कर विजयी हुए। परन्तु एक बार शत्रु से घमासान वीर युद्ध करने पर भी ह़ार गए।तब अपने शौर्य के कारण मदमत उनका अहंकार सारा मटियामेट हो गया lउसके बाद सेनापति कनक अधिकार में होते हुए भी उनका झुकाव भगवान् के प्रति था।कुछ समय के बाद माँ और पत्नी का देहावसान हो जाता है। वे विजयनगर के राजगुरु व्यास् राय के शिष्य बन गए। गुरु की आज्ञा पर उडुपी के सौदे मठ के श्रीवादिराज जी के अनुग्रह से कनकदास नामांकित किया गया।कहा जाता है कि अन्य पुण्य क्षेत्रों का संदर्शन कर अनेक कीर्तनों की रचना की। सकल क्षेत्रों की यात्रा कर उडुपी आने पर परिचारिकों के कारण श्रीकृष्ण के दर्शन नहीं हो पाया।सामाजिक भेद-भाव के कारण इन्हें दर्शन करने की अनुमति नहीं थी।तब मंदिर के बाहर पश्चिम दीवार के पास भागवत भजन, गाना शुरू कर दिया। इनकी भक्ति, श्रद्धा, संगीत और प्रस्तुति के कारण भगवान् की मूर्ति स्वयं ही इनकी तरफ घूम गयी और कनक दास ने भगवद दर्शन दिए।रूढ़िवादी समुदाय को हैरान कर दिया कि ऐसा क्यों हुआ। तब से उडुपी के श्रीकृष्ण मंदिर में श्रीकृष्ण पश्चिम की ओर मुख किए हुए है, हालांकि मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है। आज भी उडुपी के श्रीकृष्ण मंदिर में जाने वाले भक्त एक छोटी सी खिड़की जिसे “कनकना किंडी”कहा जाता है, के माध्यम से भगवान कृष्ण के दर्शन करते है।
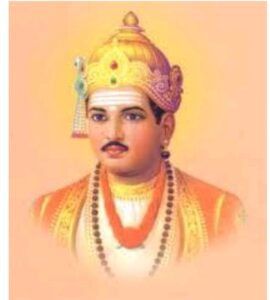
कनकदास की रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं।इनकी रचनाओं में सभी मनुष्य समान हैं, सभी का जन्म समान रूप से शारीरिक रूप से होता है। सभी समान जल साझा करते है और एक ही सूर्य को पृथ्वी पर जीवन की सहायता करते हुए देखते है, इत्यादि।इसके अलावा, उन्होंने वंचित समुदायों को दबाने वाले हठधर्मी समुदायों को कम करके एक समाज सुधारक के रूप में काम किया है।कनकदास ने अपनी सदियों पुरानी सामाजिक प्रथाओं को छोड़ने और बदलती दुनिया के अनुकूल होने के लिए वंचित समुदायों को सुधारने के लिए अत्यधिक प्रयास किया।वे अपने अंतिम दिनों में तिरुपति में रहे।

निष्कर्ष यह है कि कर्नाटक की संत परम्परा ने बोलचाल की भाषा को काव्य माध्यम बनाकर जनता की निराशा को दूर करने का प्रयास किया । इसके साथ ही स्वस्थ समाज निर्माण का दायित्व निभाया।अपनी नवीनता और मौलिकता के कारण जनमानस में स्थायी महत्व प्राप्त किया है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। सामाजिक-धार्मिक सुधारकों द्वारा समाज में विभिन्न तरह से भगवान की भक्ति का प्रचार -प्रसार किया गया। इन संतों ने भक्ति मार्ग को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते हुए “ज्ञान तथा “भक्ति” और “समन्वय “को स्थापित करने का प्रयास किया।

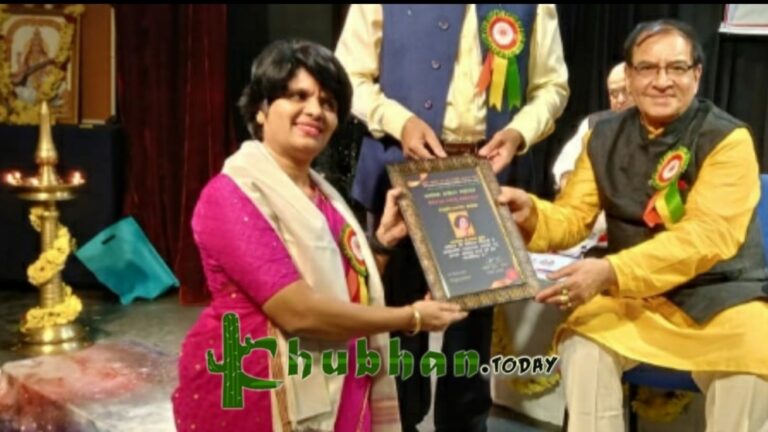

परंपरा हमारे देश का आध्यात्मिक वैभव है
Bhavna di thanks jo aap itne achche logon ki baatein hum tk pahunchti hain . Or ma’am ne bht achche se shaiv mat or vaishnav mat k upar btaya hai . Kannada bhashi hone k bawajood Hindi kitni pyari boli hai . Please Allama Prabhu k baare mein or btayein ma’am se request kariyega .